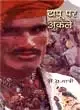|
सामाजिक >> बैरंग खत बैरंग खतसे. रा. यात्री
|
391 पाठक हैं |
||||||
‘बैरंग ख़त’ वह आईना है जिसमें लेखक ने अपने समाज के बहुविध सन्दर्भों को तेज व्यंग्य की धारदार भाषा में व्यक्त किया है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘बैरंग ख़त’ उपन्यास भारत के उस विसंगति पूर्ण वर्तमान की एक खौफनाक कहानी है जिसमें ध्वस्त होते नैतिक मूल्य, मानदण्ड
तथा मानवीय संवेदन के निरन्तर सूखते चले जाने का आख्यान निहित है। शिक्षा
का गिरता स्तर और स्वदेशी का विलोम भी इस कहानी की मुख्य धारा है।
असुरक्षित, पराजित तथा क्षुब्ध जनता दिशाहीन भीड़ बन कर रह गई है। उपन्यास
का नायक तथाकथित नैतिक पाखंडों और आग्रहों से जूझते हुए चेहरा-विहीन जनता
की नियति स्वीकार कर लेता है।
‘बैरंग ख़त’ वह आईना है जिसमें लेखक ने अपने समाज के बहुविध सन्दर्भों को तेज व्यंग्य की धारदार भाषा में व्यक्त किया है।
‘बैरंग ख़त’ वह आईना है जिसमें लेखक ने अपने समाज के बहुविध सन्दर्भों को तेज व्यंग्य की धारदार भाषा में व्यक्त किया है।
1
मेरे बड़े भाई साहब उम्र में मुझसे कोई बीस-बाइस साल बड़े
रहे होंगे। उनकी नहरवाई में एक छोटी-सी नौकरी थी—आबपाशी पतरौल की।
उनका गाँवों का दौरा रहता था। अक्सर वह आठ-दस गाँवों में अपनी खड़खड़िया
साइकिल पर ही घूम आया करते थे। बाद में जब वह अमीन साहब के पद पर
प्रोन्नति पा गये थे तो उन्हें एक मरियल-सी घोड़ी सात-आठ रुपये में खरीद
ली थी। आप आज आठ रुपये में घोड़ी खरीदने की बात पर विश्वास न कर पायें
लेकिन क्या कीजिएगा जब उस जमाने में उनकी तनखा ही कुल जमा दस रुपये माहवार थी और एक माह की तनखा में एक सैकिंडहैंड घोड़ी मिल जाती थी।
जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, वह उम्र में मुझसे कुछ इतने ज्यादा बड़े थे कि मैं उन्हें भाई के बजाय अपना पिता ही समझता था और भाभी को अपनी माँ। इसकी एक वजह शायद यह भी थी कि माता-पिता बड़े भाई के यहाँ हमेशा नहीं रहते थे। रहते थे तो बहुत बर्बरता से लड़ पड़ते थे। इसलिए उनमें से कोई कभी एक भाई के पास तो कोई दूसरा किसी और के पास रहता था। मैं उन बूढ़े-बुढ़ियों को अच्छी –खासी उम्र तक अपने माता-पिता स्वीकार नहीं कर पाया।
दसवीं कक्षा तक तो मैं भी दूसरे लड़कों की तरह, गाँव के कस्बे से स्कूल तक पैदल ही पढ़ने जाया करते था, मगर जैसे ही मैंने कालिज में दाखिला लिया, बड़े भाई साहब ने कस्बे में मामूली से किराये पर एक मकान ले लिया और मेरी माता जी को पढ़ने वाले बच्चों के पास रख दिया।
इण्टरमीडिएट में पहुँचने से पहले ही मुझे न जाने कब कविता का रोग लग चुका था। मेरा खयाल था कि मैं अकेला ही कविताकामिनी के बाल-जाल में फँसा हूँ पर बाद में पता चला कि सत्रह-अठारह की उम्र के अनेक कालिजियेट इस रोग से पीड़ित थे। एक तो कविवर सुमित्रानन्दन पन्त की तर्ज पर न केवल उनकी तरह लम्बे बाल छितराये घूमते थे बल्कि बी.ए. के प्रथम वर्ष में ही इलाहाबाद में जाकर उनसे बाकायदा मिल आये थे। उनका पंत जी से मिलना क्या हुआ वह तो कपड़े भी पंत जी जैसे ही पहनने लगे और उनकी कविताओं के छन्द और शब्दावली भी हू-ब-हू पंत जी जैसी हो चली।
बी.ए. तक तो महज कविता लिख-पढ़ ही ली जाती थी पर ज्योंही एम.ए.(हिन्दी) के प्रथम वर्ष में दाखिला लिया, कविता सिर पर भूत जैसी चढ़ बैठी। हालत यहाँ तक बिगड़ी कि बरसात की रातों में सोते समय घने अन्धकार के बीच पिछवाड़े की तरफ मेढक टर्राते या झींगुर की झनझन सुनाई पड़ती तो मैं अपने सिरहाने से कापी-कलम खींचकर विरह-वेदना के गीत लिखने बैठ जाता। चारों तरफ गहरा अँधेरा छाया होता और मैं जंगले पर बैठा दूर तक फैले जंगल को आँखें फाड़-फाड़कर निहारता रहता। दिखता-दिखाता तो उस कालेपन में क्या होगा—हाँ कागज पर अन्दाज से कुछ न कुछ घसीट लेता था और सुबह सट्टे के नम्बरों की तरह उन टेढ़े-मेढ़े शब्दों का कुछ अर्थ निकालने की कोशिश करता था।
मेरा पंतानुरागी मित्र बी.ए. पास करते ही अपनी पत्नी और कविता दोनों को अपने साथ लेकर –दिल्ली में जा बसा था। वहाँ उसे एक मामूली-सी क्लर्की मिल गई थी। कभी-कभी बीच में एक-दो रोज के लिए वह दिल्ली से आया करता था तो हम लोगों को बतलाया करता था कि वह अपनी कविताएँ रेडियो से सुनाता है और उसकी कविताओं को गाने के लिए भी रेडियो वालों से अनुबंध हो चुका है।
यों तो उसकी इन बातों से सभी चमत्कृत होते थे पर मैं तो उसकी सूचनाओं से दिवास्वप्नों में गोते खाने लगता था। मैं सोचने लगता था कि क्या कभी मेरे जीवन में भी कोई ऐसी शुभ घड़ी आयेगी जब मुझे रेडियो वाले कविताएँ सुनाने के लिए आमंत्रित करेंगे।
कई बार मेरी, अपने दिल्ली निवासी मित्र से यह कहने की इच्छा होती थी कि वह मुझे भी एक बार रेडियो से कविताएँ सुनाने का निमंत्रण दिलवा दे लेकिन यह बात मैं उससे कभी कह नहीं पाता था। एक तो अपने लिए कहते संकोच होता था, दूसरी बात यह थी कि मैं अपने बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं था कि मैं वास्तव में कवि हूँ भी या नहीं।
उस वक्त तक मेरी कविताएँ कहीं छपी तो नहीं थीं पर कालिज और कस्बे में ‘कविजी’ कहके पहचाना जाने लगा था। होते-होते इस बीमारी के लक्ष्ण इतने उभरे कि मेरे घर परिवार के लोगों को भी मेरी असाध्य बीमारी का पता चल गया। यह कुछ अनायास ही हो गया। जाड़े के मौसम में इधर-उधर के शहरों-कस्बों में पता नहीं कौन लोग कवि सम्मेलनों और मुशायरों का आयोजन करते थे और थोड़ी-सी फीस यानी आने-जाने का किराया देकर मेरे जैसे सीखतड़ (नौसिखुए) को भी निमंत्रण पत्र भेज देते थे। इन आयोजकों की असीम अनुकम्पा से ही मुझे आस-पास के जिलों में बुलाया जाने लगा और और हिन्दी साहित्य में एम.ए. पास करते-करते मैं कवि घोषित कर दिया गया।
जब मैं निष्काम एम.ए. पास था तो दो ही कार्य सामने थे। पहला, अखबारों की ‘जरूरत’ के अनुसार नौकरी के लिए आवेदन-पत्र लिखकर भेजना। दूसरा बिना लाइन के कागज पर सुलेख में गीत अथवा कविता लिखकर साप्ताहिकों और मासिकों के सम्पादकों के पास भेजना। उनकी गति-मति की भूरि-भूरि प्रशंसा भी कविता के साथ लिखनी होती थी पर वह कुछ इतने क्रूर हृदय होते थे कि सप्ताह बीतते न बीतते ‘सधन्यवाद’ वापस की एक छपी किट कविता के साथ चेंपकर मेरी काव्यकामिनी को मेरी ओर ही धकेल मारते थे। यह लुका-छिपी कुछ इतनी दीर्घसूत्री थी कि मैं अपने कवि होने पर संदेह करने लगा।
कुछ हो कविता में और कुछ हो न हो—एक बात तो होती है कि जब इसकी धुन लग जाती है तो आसानी से छुड़ाये नहीं छूटती। दूसरे-दूसरे सभी कामों से आप कभी-न-कभी भाग खड़े हो सकते हैं पर एक बार कवि कहलाने के बाद आप इसका यश किसी तरह नहीं छोड़ना चाहते।
सहसा इसी समय मेरा भाग्योदय होने का एक आभास मिला। मेरे बड़े भ्राता जो गाँव में रहते थे और अमीनी करते थे, एक दिन कस्बे के घर में आकर बोले, ‘‘ले भाई तेरे कबीर जी (कवि जी) होने की बात तो हमने ऊपर तक पहुँचा दी।’’
मेरे ज्येष्ठ भ्राता मात्र मिडिल पास थे और उन्हें कवि और कबीर में कोई अन्तर मालूम न था। उनके लिए तुलसीकृत रामायण के अलावा और कहीं कविता नहीं थी और तुलसीकृत रामायण को वह भले ही लाल कपड़े में बड़ी श्रद्धा से बाँध-बूँधकर सँभालकर रखते हों पर तुलसी के कवि होने की गरिमा से वह रत्ती-भर प्रभावित नहीं थे। उन ऐसे भक्तप्रवर अनुज से अपने कवि होने की स्वीकृति पाना ही कुछ कम नहीं था—यह जो अपने नाम के ऊपर तक पहुँचने की बात सुनी तो मेरा सिर घूम गया। कई मिनट तो मैं सकते की हालत में रहा कि वह क्या कह रहे हैं पर अन्ततः मैंने सही बात जानने की गरज से उनका चेहरा देखा—पूछा कुछ नहीं। दरअसल उस जमाने में अपने से उम्र में बड़े गुरुजन से कुछ पूछने की परम्परा नहीं थी, इसे बड़ों से ‘जुबान लड़ाना’ समझा जाता था। जो कुछ और जितना कुछ वह बतला-समझा देते थे—काफी समझा जाता था।
मुझे अपनी ओर ताकते देखकर वह गर्व से हँसे और कहने लगे, ‘‘धरपा गाँव का चौधरी एदल सिंह रेडियो स्टेशन पर एक बड़ा अफसर है—डायरेक्टर समझो। मैंने उससे तेरा जिकर किया था। कधी-कधा गाँव में आत्ता रहवे है। कहरा था कि उसे कधी दिल्ली बेज्जो अपनी लिखी कबीता लैके।’’ फिर वह निष्कर्ष देते हुए बोले, ‘‘वो तेरी कविता, रेडियो पै गवा देगा जरूर। इब वैसे बी तू तू कुछ कर तो रहा नी—अपनी कविता ठाके (उठाकर) चला जा किसी दिन—मन्ने तो तेरी भतेरी तारीफ कर रक्खी। न्यूँ बी दिल्ली कुछ घणी दूर तो हैनी।’ किरावा बी कुछ ढेर नी लगता। सुबेरे की गड्डी पकड़ लियो जकशन पै जाके। परोगराम करके रात की टरेन से वापस चल पड़ियो।’’
यह जो रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर साहब से सीधे ही जा मिलने की जुगत निकली तो कई दिनों तक मैं पूरी तरह से बौखलाया घूमता रहा। मैं उन दिनों खद्दर का कुर्ता-पायजामा और जाड़ों में कश्मीरी पट्टू की सदरी जिसे सब जवाहरकट कहते थे—पहना करता था। खूब लम्बा और गोरा-चिट्टा युवक था पर दिल्ली के रेडियो पर बड़े अफसर से मिलने के लिए तो जरा ढंग की पोशाक चाहिए थी। और लिबास भी कुछ ऐसा जो वहाँ की दुनिया में उजबक घोषित न करे।
अब से चालीस-पैंतालीस बरस पहले एक खास कपड़े का सूट पहनने का रिवाज था, उसे गैबरडीन कहते थे। मेरे सौभाग्य से मेरे भाई ओवरसियर थे। पी.डब्लू.डी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट एक सोने का अण्डा देने वाली तगड़ी मुर्गी समझा जाता था और वह उसी में—आज की भाषा में—जूनियर इंजीनियर थे। मेरे भाई-भाभी उस दौरान एक बार हम लोगों से मिलने आये हुए थे। मुझे हल्के से कुर्ते पायजामें में देखकर मेरी भाभी को बड़ी दया आई और उन्होंने तुरन्त अपने बटुए से सौ रुपये का नोट निकाल कर मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, ‘‘भैया जी आप एक सूट बनवा लो गैबरडीन का।’ वह एकदम निरक्षर होते हुए भी आदमी को सूट पहनने पर ही आदमी मानती थीं। मेरा स्वदेशी प्रेम रुपये पाते ही न जाने कहाँ हवा हो गया। मैं उड़ता हुआ कंछीलाल बजाज की दुकान पर गया।। सूट के लिए गैबरडीन कटवाई और कंछीलाल के ठीक सामने वाले शेर खाँ दर्जी, जिसे आम तौर पर मास्टर कहा जाता था, को जा पकड़ाई।
मास्टर शेर खाँ ने एक हफ्ते के बाद ट्राई के लिए आने को कहा और मेरा नाप लेते हुए बोला, कपड़ा कुछ बेसी है—एक टोपी भी निकल आयेगी।’
मास्टर शेर खाँ की बात पर मैं मन ही मन हँसा—यहाँ सूट-टाई पर कौन मरदूद टोपी लगायेगा ? मगर मुझे बाद में यह देखकर तो अनेक बार हैरानी हुई कि हमारे कस्बे में ही नहीं, इस महान देश के बड़े-बड़े नगरों तक में न जाने कितने धर्म-प्राण सूट के नीचे जनेऊ और नेकटाई के बावजूद सिर पर चोटी-टोपी बड़ी शान से धारण करते हैं। यही नहीं किसी मंदिर, शिवालय या दो ईंटे खड़ी करके भूमिया के थान के सामने बाकायदा हाथ जोड़कर श्रद्धाभिभूत हो सिर नवाते हैं।
पहले तो मैंने सोचा, अपने दिल्ली निवासी मित्र कवि शैलेश को पत्र लिखकर रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर चौधरी एदल सिंह के बारे में पता करूँ और हो सके तो उसी के साथ जाकर उस नामी-गिरामी हस्ती के शुभ दर्शन करूँ। शैलेश निश्चय ही उनसे थोड़ा-बहुत परिचित तो होगा ही। फिर उसकी रेडियो स्टेशन तक सहज पहुँच भी थी। उसके साथ जाने पर कहीं भटकने की ज्यादा गुंजाइश भी नहीं थी क्योंकि उसे दिल्ली में रहते दो-ढाई साल हो चुके थे।
परन्तु काफी सोच-विचार करने के बाद मुझे लगा कि शैलेश के साथ चौधरी एदल सिंह जी से मिलने जाना ठीक नहीं होगा। हो सकता है, वह इस बात को पसन्द ही न करें कि उन्होंने मिलने के लिए बुलाया तो मुझे और मैं एक और को साथ टाँग कर ले गया। इसके अलावा मैं गुपचुप ढंग से रेडियो की इस तोप से मुलाकात करके शैलेश पर कहीं यह रोब भी डालना चाहता था कि बच्चू रेडियो से कविताई गाने वाले तुम अकेले तुर्रम खां नहीं हो—मुझे भी रेडियो वाले तुमसे कहीं बेहतर ढंग से घास डालते हैं। मैं चाहता था कि रेडियो से धूमधाम मचाने वाला मेरा एक कार्यक्रम प्रसारित हो जाए तो मैं अपने सहपाठी और प्रतिद्वन्द्वी को ऊँट बनाकर पहाड़ के नीचे से निकाल दूँ।
मैं निश्चित दिन और तारीख पर मास्टर शेर खां की दूकान पर गया और काफी तनते उचकते हुए टेलर मास्टर को सूट की ‘टिराई’ दे आया। रात-दिन सपनों में डूबते-उतराते वक्त गुजर रहा था। हालाँकि मैंने अभी तक रेडियो स्टेशन की इमारत तो क्या उसकी कहीं एक तस्वीर तक भी नहीं देखी थी, मगर मैं अपने मानसिक नेत्रों से उसे सुने-सुनाये भवन के गलियारों और स्टूडियो के चक्कर काटता फिरता रहता था और लौट कर चौधरी एदल सिंह रेडियो स्टेशन डायरेक्टर के शानदार कक्ष में उनके सामने कुर्सी पर जा बैठता था और घोर आत्मीयता से वार्तालाप करता रहता था। मेरा यह हवाई बतियाना जब शिखर पर था तभी एक दिन शैलेश दिल्ली से आ निकला। उसने कस्बे की मानसिकता पर लानत भेजते हुए दिल्ली में अपनी उपलब्धियों की फेहरिस्त मेरे सामने फैला दी। वह वहाँ कितने बड़े-बड़े राजनेताओं और संसद सदस्यों तथा साहित्यकारों से आये दिन मिलता रहता है तथा उसे वहाँ साहित्य का मंच अनायास उपलब्ध होता रहता है, इसका उसने ‘आपन भरनी आपन करनी—विविध मुख बरनी’ की तर्ज पर घंटों बखान किया। उसकी बातों को लनतरानियों का बेसिर का पिटारा मानकर—उसकी बातों पर मैं मन-ही-मन बहुत ऊँचाई पर बैठा हँसता रहा। मैंने उसे रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर से मिलने की इच्छा और योजना की हवा भी नहीं लगने दी। हाँ, चालाकी से यह अवश्य पूछ लिया कि यह भवन दिल्ली में कहाँ स्थित है और इसमें लोग किस तरह दाखिल होते हैं।
शैलेश, अपनी भविष्य निधि के तौर पर फैली अनेक योजनाओं का विराट स्वरूप मुझे दिखाकर दो-चार दिन में ही दिल्ली वापस लौट गया। इधर मैंने भी भाभी से मिले सौ रुपयों का शेषांश—पच्चीस रुपया टेलर मास्टर शेर खां की नजर करके उनके कारखाने से अपना गैबरडीनी सूट उठा लिया। मैं लाख भूलना चाहूँ मगर मास्टर शेर खाँ टोपी-क्षेपक नहीं भूला। उसने सूट लिफाफे में डालने के बाद टोपी मेरे हाथ में देते हुए कहा, ‘‘जनाबेमन शायर साहब, यह टोपी आप की शख्शियत में चार चाँद लगा देगी। माशाल्ला जरा लगाकर तो दिखाइये।’’
टोपी के प्रति घोर वितृष्णा का भाव मन में धीरे-धीरे भी मैंने सामने के आदम-कद आइने में खुद को नापते-तौलते हुए भी सूट से कहीं पहले उस सितम जरीफ़ टोपी को सिर पर चढ़ाकर दाएँ-बाएँ खिसकाया और स्वयं पर सैकड़ों लानतें भेजते हुए उस टोपी को सिर से उतारकर दीवार के सहारे खड़ी सिलाई मशीन पर टिका दिया और वहाँ से यों लपका जैसे कोई जेबकतरा भीड़ में गुम होने के लिए सिर पर पाँव रखकर भाग खड़ा होता है।
सूट मिल जाने के बाद भी मैं तुरन्त दिल्ली नहीं जा सका क्योंकि जिन्दगी में पहली बार मेरा सूट सिला था। उसे पहनने का अभ्यास जरूरी था। मैंने कभी टाई और गर्दन का मेल-मिलाप भी नहीं देखा जाना था—उस स्थिति को भी जानना समझना था। इसके अलावा फ्लैक्स के जूतों की जो एक बड़ी दूकान शहर में थी, उस पर जाकर अपने खुरपे जैसे लम्बे बेडौल पैरों के लिए बूट जुटाने की मुहिम भी सर करनी थी और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि मैं अपने किसी परिचित अथवा मित्र को भी इस डर से अपनी सहायतार्थ नहीं घेर सकता था कि कहीं वह मेरे इस नये शौक का मखौल उड़ाते हुए इसे ‘टाक आफ दा टाउन’ की रंगत न दे दे।
रम्मू फ्लैक्स वाले की दूकान बन्द होने से पहले मैं गली के कोने पर जाकर खड़ा हो गया और जब मैंने देखा, रम्मू के अलावा उसके शोरूम में सिर्फ जूतों पर चँवर डुलाने वाला छोकरा ही बाकी रह गया है तो मैं गली से निकल कर सड़क पर जा निकला और रम्मू के जूतों की अलमारियों के बीच जाकर खड़ा हो गया। अनाज की पूरमपूर दो बोरियों को एक के ऊपर रख दिया जाय तो रम्मू के आकार-प्रकार और आगे बढ़े पेट का कुछ अन्दाज हो सकता है। रम्मू ने अपनी आँखें मिचमिचाते हुए मेरी मंशा की थाह ली और लड़के से बोला, ‘‘छंगा ! बाबूजी को जूता दिखा।’’ पर उसके कण्ठ की घरघराहट से शब्द यों सुनाई पड़े, ‘‘छंगा ! बाजूजी कू जूता सुँघा।’’
किसी तरह ग्यारह रुपये में मुझे पता नहीं किस कम्पनी (फ्लैक्स का जूता) उस जमाने में भी चौदह-पन्द्रह से कम नहीं मिलता था) का बूट रम्मू ने भेड़ दिया। भले ही उसकी दूकान पर फ्लैक्स का जहाजी बोर्ड लगा था मगर माल उसके यहाँ हर छोटी-बड़ी कम्पनी का मौजूद था।
यह एक अलग कहानी है कि उन बूटों ने हफ्तों तक परम शत्रु का व्यवहार ही नहीं किया जब भी मौका पाया मेरे टखनों तक को स्नेहभाव से कुछ इस ढब पर सहलाया कि आज तक टखनों की खाल काफी ऊपर तक खिंच जाने पर भी उन संस्पर्शों से चिह्नित है। एड़ियों की कटाई-मंजाई से उद्भूत छालों की गाथा तो ‘छिल छिलकर छाले फोड़े’ तक भी जा पहुँची थी। बाद में मेरी दीन दशा पर एक प्रत्यक्षदर्शी का सुझाव था कि ऐसे बीहड़ पादत्राणों की मार से बचने के लिए मोटी-तगड़ी जुराबें पहनने का शऊर पैदा करना भी जरूरी है।
कोट की ऊपरी जेब में गुलाबी रूमाल अटकाने से लेकर गले में टाई लटकाने तक के लिए भी बाकायदा एक ‘मास्टर आफ साइंस’ की शिष्यता ग्रहण की जब मैं टाई में किसी तरह भी कायदे की ‘नाट’ नहीं लगा सका तो उन्होंने हारकर सर्पीली धजा वाली टाई को अपने गले में डालकर उसमें गाँठ लगाई और गले से टाई निकालकर मेरे हाथ में देते हुए आजिजी से बोले, ‘‘अब इसे इसी हालत में सँभाल कर रखो। जब पहनने की जरूरत पड़े तो गले में डालकर इसकी निचली पर्त खींच देना—बिल्कुल फाँसी के फन्दे की तरह।’’
सूट-बूट-टाई-रूमाल और जाड़े का मौसम आ जाने की वजह से कोट के बटन होल में गुलाब की कली अटकाने का कई दिनों तक अभ्यास करने के बाद मैंने दिल्ली जाने की सोची। जाने से पहले एक महत्त्वपूर्ण कार्य उन कविताओं और गीतों को ढंग से सँजोना-सँवारना भी था जो ‘आल इंडिया रेडियो’ के स्टेशन डायरेक्टर साहब को सौंपे जाने थे। मैंने बाजार से हल्के नीले कागजों का एक बड़ा पैड खरीदा और कई दिनों तक सुलेख में उन पर बड़ी सधी उँगलियों से अक्षर-अक्षर कविताएँ उभारीं। मैं अपनी कविता की बेड़ियों में चौधरी एदल सिंह को पूरी तरह जकड़ लेना चाहता था।
उस जमाने के हिसाब से जो भी सुन्दरतम हैन्डबैग बाजार में मिल सकता था, उसमें मैंने कविताओं का पैड जमाया और एक छोटी-सी अटैची में एक-दो कपड़े, रूमाल, कंघा आईना और ‘अफगान स्नो’ की शीशी रख ली और एक सुबह घर से दिल्ली विजय के अभियान पर निकल पड़ा।
रिक्शा स्टैण्ड तक मैं कई छोटे-छोटे शार्टकट पार करके पहुँचा और मैंने अपनी आँखें बराबर नीचे झुकाए रखीं। एक तो मैंने इस तरह सरेआम सूट-बूट टाई वगैरह पहले कभी नहीं पहनी थी, दूसरे मैं अपनी शुभयात्रा के आरम्भ में ही किसी की टोका-टाकी का सामना करना नहीं चाहता था।
मैं अपने लिबास को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क था, पर मुसीबत यह थी, कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी मेरे कस्बे से चार मील दूर जंक्शन से मिलती थी। न तो मैं उस लिबास में चार मील धूल-धक्कड़ में पैदल चल सकता था, न ताँगे में बाकी आठ सवारियों के बीच ठुँस सकता था। सड़क की हालत का तो बस कहना ही क्या। हर दस-बारह गज के फासले पर बेमाप गढ़े-गढ़हिया नजर आते थे। शेरशाह सूरी के जमाने में द्द्धी की सड़क थी। कहा जाता है कि जब सन उन्नीस सौ छियालीस में पंडित नेहरू कस्बे में आये थे तो उन्हें दूसरे कई उपहारों के साथ सिख समाज ने सरोपा, एक तलवार भी भेंट की थी। जब पंडित जी का काफिला पंडितजी को इलाहाबाद की गाड़ी पर सवार कराने के लिए जंक्शन की ओर रवाना हुआ तो पंडित जी कार के बार-बार रुकने की वजह जानने के लिए कार से बाहर निकल आए थे और उन्होंने गाँव के कच्चे रास्तों से भी गई-बीती सड़क का जायजा लेते हुए हाथ में पकड़ी हुई तलवार को हवा में लहराते हुए क्रोधावेश में घोषणा की थी, ‘‘अगर किसी दिन मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो मैं इस कस्बे के चेयर मैन को फाँसी लगवा दूँगा।’’
जिस समय का मैं जिक्र कर रहा हूँ तब तक पंडित जी को इस देश का प्रधानमंत्री बने कई साल गुजर चुके थे। एक आम चुनाव भी देश में वर्षों पहले सम्पन्न हो चुका था मगर न तो हमारे कस्बे की म्यूनिसिपैलिटी के चेयर मैन को फाँसी पर चढ़ाया गया था न उस सड़क की हालत में कोई तब्दीली हुई थी। अब मैं जेब में गुलाबी रुमाल दबाये सोच रहा था कि जंक्शन तक बिना धूल का पाउडर पोते कैसे पहुँचूँ। बस एक ही रास्ता था कि भाड़े पर पूरा रिक्शा लूँ और कस्बे से निकलने के बाद सड़क से हटकर पतली-सी पगडण्डी पर हौले-हौले रिक्शा चलवाते हुए जंक्शन तक पहुँचूँ। इसमें बस खतरा यही था कि जिस गाड़ी को पकड़ने की नीयत से मैं घर से निकला था, वह मुझे न मिल पाती। ‘अब जो भी हो—देखा जाएगा’ के भाव से मैंने एक रिक्शाचालक से अकेली सवारी ले चलने की पेशकश की और उस पर सवार होकर चल पड़ा।
जैसा सोचा था वही हुआ। नौ बजे की गाड़ी तो उसी समय छूट गई जब मैं रेलवे स्टेशन से लगभग डेढ़ मील दूर था। अब इलाहबाद की तरफ से ग्यारह बजे के करीब एक डाक गाड़ी आती थी उसी के मिलने की उम्मीद थी। रेलवे स्टेशन पर पहुँच कर मैंने बहुत सावधानी से अपने सूट पर पड़ी धूल की महीन पर्त को हल्के हाथों से झाड़ा और रिक्शा का भाड़ा चुकाकर दिल्ली का टिकट खरीदने खिड़की के सामने पहुँच गया।
साधारण दर्जे का टिकट खरीदने के लिए तब तक छोटे कस्बों के स्टेशनों पर ‘क्यू’ सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। मार ठट्ट के ठट्ठ देहाती और कस्बाई भीड़ टिकट खिड़की पर पिली पड़ रही थी। मैंने भीड़ में घुस कर टिकट खरीदने का जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा। उससे तो मेरे कोट-पतलून का भुरकुस ही निकल जाता। लिहाजा मैंने अपने रिक्शाचालक को एक अठन्नी का लोभ देकर दिल्ली का तीसरे दर्जे का टिकट खरीदवाया। यह बाद की बात है जब रेलवाई ने तीसरे दर्जे के एक डंडे को हटाकर उसे झूठ-मूठ में ही सेकिंड क्लास कर दिया था।
पुरानी दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी से उतर कर मैं प्लेटफार्म पार करके बाहर सड़क पर आया तो बेपनाह भीड़ देखकर बौखला-सा गया। मेरा दिल्ली का भौगोलिक ज्ञान लगभग शून्य था। बहुत साल पहले दिल्ली में जब मेरे भाई सी.पी.डब्लू.डी. में कुछ सालों तक जूनियर इंजीनियर रहे थे तो मैं उनके पास आया था। अब यह भी भूल चुका था कि मैं तब किसके साथ आया था। स्टेशन से कुछ फर्लांग आगे चाँदनी चौक था और वहाँ सड़कों पर तब ट्रामें चलती थीं। मगर सुना था कि इस बीच उनका चलना बन्द हो चुका था और दिल्ली में दूर-दूर तक दिल्ली परिवहन की बसें चलने लगी थीं।
भीड़ में धक्के खाता मैं चाँदनी चौक से कुछ पहले ही ठहर गया। बहुत-सी बसें इधर-उधर दूर तक लम्बी लाइन में खड़ी थीं और उन पर उन स्थानों के नाम भी दर्ज थे जहाँ उन्हें जाना था। दस-पाँच लोगों से पूछताछ करके मैं पार्लियामेण्ट की दिशा में जाने वाली एक बस पर सवार हो गया और लगभग पौन घंटे में आल इंडिया रेडियो की उस विशेष इमारत के सामने जा पहुँचा जो उस समय तक ‘मीडिया’ की दृष्टि से इस देश की नाड़ी कही जा सकती थी।
बस से उतर कर मैंने इधर-उधर देखा और मन की धुकुड़-पुकुड़ पर काबू पाने का असफल प्रयास करते हुए आकाशवाणी भवन के सामने जाकर खड़ा हो गया।
उस क्षण मैंने पाया कि मुझमें आत्मविश्वास की गहरी कमी है और मैं गैबरडीन का बढ़िया सूट धारण करने के बावजूद निपट बेचारा कस्बाई हूँ जो पार्लियामेण्ट की स्ट्रीट की भव्य इमारतों को दीदे फाड़-फाड़ कर देख रहा है और जिसकी हिम्मत इस सीमा तक जवाब दे गई है जो किसी दफ्तर या भवन के गेट में भी नहीं घुस सकता।
कितनी ही देर तक मैं ‘आल इंडिया रेडियो’ की बिल्डिंग के बाहर खड़ा गेट से बाहर भीतर आने-जाने वालों को देखता रहा। अजीब-अजीब हुलियों और पोशाकों वाले लोग आते-जाते दीख रहे थे। किसी स्थूलाकार आकृति वाले के लम्बे और तैलाक्त बाल पीठ पर पड़े थे और प्रशस्त ललाट पर त्रिपुण्ड शोभायमान था तो उसकी बगल में तम्बूरा थामे कोई महामरियल गुड्डे जैसा व्यक्ति ओंठ चियारता हुआ नजर आ रहा था। कहीं कोई सूखी लकड़ी जैसी रमणी गेट के बाहर निकल रही थी तो बंगाली काट का कुर्ता और चुन्नटदार धोती का कोना कुर्ते की जेब में फँसाये बंगाली मोशाय लपकते नजर आ रहे थे। मैंने थोड़ी देर में ही समझ लिया कि अखिल भारतीय आकाशवाणी पर अखिल भारतीय प्रतिभाओं का जमावड़ा स्वाभाविक है। किसी भी आने-जाने वाले को अपने से अलग किसी का अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता था। स्वयं या अपने साथ के लोगों के वजूद के अलावा दूसरों से लगभग सभी पूरी तरह बेखबर थे।
गेट के बाजू में पान की दूकान थी जिस पर खासी भीड़ जमा थी। चूँकि तब तक मेरा पान-बीड़ी-सिगरेट से कुछ लेना-देना नहीं था, इसलिए हिम्मत करके पनवाड़ी से कुछ पूछना भी संभव नहीं था। अन्त में हिम्मत करके एक खाकी वर्दी वाले दरबान या गेटकीपर से मैंने चौधरी एदल सिंह से मिलने की बात कही। वह शख्स भी देहात का रहने वाला क्योंकि उसने अपनी बीड़ी जलाना छोड़कर गौर से मुझे देखा और मेरे सूट के भीतर बदहवास देह-प्राण की मुश्किल का अन्दाज लगाकर भले मानुष का रूख अख्तियार कर लिया। ‘‘लगता है चौधरी के मनई हओ—सूधे जायकै स्टूडियो के दुआर पै पहोंचौ। चौधरी हुंई मिल जाई चहै।’’
मेरी मुश्किल इतनी आसानी से हल हो जायगी, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं समझता था चौधरी एदल सिंह जैसे बड़े और महत्त्वपूर्ण अधिकारी से मिलने में पता नहीं कितनी बाधाएँ उपस्थित होंगी।
मैं आश्वस्त होकर आगे बढ़ते हुए एक लम्बे गलियारे में घुस गया और गलियारे के बीच में खड़े एक खाकी वर्दीधारी अधेड़ से पूछने लगा, ‘‘मुझे चौधरी एदल सिंह जी स्टेशन डायरेक्टकर से मिलना है—क्या बता सकते हैं कि वह कहाँ मिलेंगे ?
भारी-भरकम देह वाले उस रोबीले गेटकीपर ने मुझे पैरों से सिर तक बड़े ध्यान से देखा और फिर उसके चेहरे पर विचित्र-सी मुस्कराहट दीख पड़ी। उसकी मुस्कान में परिहास की कमी नहीं थी। वह गम्भीर होने का प्रयास करते हुए बोला, ‘‘तो डायरेक्टर साहब चौधरी जी से मिलने आये हो।’’
मेरे ‘हाँ’ कहने पर उसने गलियारे से गुजरते अपने जैसे लिबास वाले एक नौजवान को आवाज दी, ‘‘नोखे लाल, इन साब कू डिरेक्टर चौधरी जी के पास तो छोड़ अइयो—देख वहीं स्टूडियो के गेट पै स्टूल पै बैठे होंगे स्यात।’’
गेटकीपर के इन शब्दों का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया कि चौधरी जी स्टूडियो के गेट पै स्टूल पै बैठे होंगे स्यात। पर मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान न देकर नोखे लाल के पीछे चलने की ही कोशिश की।
मैं यह देखकर ताज्जुब में पड़ गया कि गोल गुम्बद के नीचे गोलाकार भाग को पार करते ही स्टूडियो के प्रवेश द्वार पर जो मझले कद का अधेड़ व्यक्ति खड़ा था—नोखे लाल मेरी ओर संकेत करके उससे कुछ कह रहा था।
मैं वहाँ पहुँचा तो वह ताँबई रंग और कद्दावर काठी वाला आदमी जरा आगे बढ़ आया और बोला, ‘‘अमीन साब के लोहरे (छोटे) भैया हो ? उनने मोय बतायो हतौ कि हमाओ भैया कबीर है गयो—वाय कबीता की लत लग गई हतै।’’
जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, वह उम्र में मुझसे कुछ इतने ज्यादा बड़े थे कि मैं उन्हें भाई के बजाय अपना पिता ही समझता था और भाभी को अपनी माँ। इसकी एक वजह शायद यह भी थी कि माता-पिता बड़े भाई के यहाँ हमेशा नहीं रहते थे। रहते थे तो बहुत बर्बरता से लड़ पड़ते थे। इसलिए उनमें से कोई कभी एक भाई के पास तो कोई दूसरा किसी और के पास रहता था। मैं उन बूढ़े-बुढ़ियों को अच्छी –खासी उम्र तक अपने माता-पिता स्वीकार नहीं कर पाया।
दसवीं कक्षा तक तो मैं भी दूसरे लड़कों की तरह, गाँव के कस्बे से स्कूल तक पैदल ही पढ़ने जाया करते था, मगर जैसे ही मैंने कालिज में दाखिला लिया, बड़े भाई साहब ने कस्बे में मामूली से किराये पर एक मकान ले लिया और मेरी माता जी को पढ़ने वाले बच्चों के पास रख दिया।
इण्टरमीडिएट में पहुँचने से पहले ही मुझे न जाने कब कविता का रोग लग चुका था। मेरा खयाल था कि मैं अकेला ही कविताकामिनी के बाल-जाल में फँसा हूँ पर बाद में पता चला कि सत्रह-अठारह की उम्र के अनेक कालिजियेट इस रोग से पीड़ित थे। एक तो कविवर सुमित्रानन्दन पन्त की तर्ज पर न केवल उनकी तरह लम्बे बाल छितराये घूमते थे बल्कि बी.ए. के प्रथम वर्ष में ही इलाहाबाद में जाकर उनसे बाकायदा मिल आये थे। उनका पंत जी से मिलना क्या हुआ वह तो कपड़े भी पंत जी जैसे ही पहनने लगे और उनकी कविताओं के छन्द और शब्दावली भी हू-ब-हू पंत जी जैसी हो चली।
बी.ए. तक तो महज कविता लिख-पढ़ ही ली जाती थी पर ज्योंही एम.ए.(हिन्दी) के प्रथम वर्ष में दाखिला लिया, कविता सिर पर भूत जैसी चढ़ बैठी। हालत यहाँ तक बिगड़ी कि बरसात की रातों में सोते समय घने अन्धकार के बीच पिछवाड़े की तरफ मेढक टर्राते या झींगुर की झनझन सुनाई पड़ती तो मैं अपने सिरहाने से कापी-कलम खींचकर विरह-वेदना के गीत लिखने बैठ जाता। चारों तरफ गहरा अँधेरा छाया होता और मैं जंगले पर बैठा दूर तक फैले जंगल को आँखें फाड़-फाड़कर निहारता रहता। दिखता-दिखाता तो उस कालेपन में क्या होगा—हाँ कागज पर अन्दाज से कुछ न कुछ घसीट लेता था और सुबह सट्टे के नम्बरों की तरह उन टेढ़े-मेढ़े शब्दों का कुछ अर्थ निकालने की कोशिश करता था।
मेरा पंतानुरागी मित्र बी.ए. पास करते ही अपनी पत्नी और कविता दोनों को अपने साथ लेकर –दिल्ली में जा बसा था। वहाँ उसे एक मामूली-सी क्लर्की मिल गई थी। कभी-कभी बीच में एक-दो रोज के लिए वह दिल्ली से आया करता था तो हम लोगों को बतलाया करता था कि वह अपनी कविताएँ रेडियो से सुनाता है और उसकी कविताओं को गाने के लिए भी रेडियो वालों से अनुबंध हो चुका है।
यों तो उसकी इन बातों से सभी चमत्कृत होते थे पर मैं तो उसकी सूचनाओं से दिवास्वप्नों में गोते खाने लगता था। मैं सोचने लगता था कि क्या कभी मेरे जीवन में भी कोई ऐसी शुभ घड़ी आयेगी जब मुझे रेडियो वाले कविताएँ सुनाने के लिए आमंत्रित करेंगे।
कई बार मेरी, अपने दिल्ली निवासी मित्र से यह कहने की इच्छा होती थी कि वह मुझे भी एक बार रेडियो से कविताएँ सुनाने का निमंत्रण दिलवा दे लेकिन यह बात मैं उससे कभी कह नहीं पाता था। एक तो अपने लिए कहते संकोच होता था, दूसरी बात यह थी कि मैं अपने बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं था कि मैं वास्तव में कवि हूँ भी या नहीं।
उस वक्त तक मेरी कविताएँ कहीं छपी तो नहीं थीं पर कालिज और कस्बे में ‘कविजी’ कहके पहचाना जाने लगा था। होते-होते इस बीमारी के लक्ष्ण इतने उभरे कि मेरे घर परिवार के लोगों को भी मेरी असाध्य बीमारी का पता चल गया। यह कुछ अनायास ही हो गया। जाड़े के मौसम में इधर-उधर के शहरों-कस्बों में पता नहीं कौन लोग कवि सम्मेलनों और मुशायरों का आयोजन करते थे और थोड़ी-सी फीस यानी आने-जाने का किराया देकर मेरे जैसे सीखतड़ (नौसिखुए) को भी निमंत्रण पत्र भेज देते थे। इन आयोजकों की असीम अनुकम्पा से ही मुझे आस-पास के जिलों में बुलाया जाने लगा और और हिन्दी साहित्य में एम.ए. पास करते-करते मैं कवि घोषित कर दिया गया।
जब मैं निष्काम एम.ए. पास था तो दो ही कार्य सामने थे। पहला, अखबारों की ‘जरूरत’ के अनुसार नौकरी के लिए आवेदन-पत्र लिखकर भेजना। दूसरा बिना लाइन के कागज पर सुलेख में गीत अथवा कविता लिखकर साप्ताहिकों और मासिकों के सम्पादकों के पास भेजना। उनकी गति-मति की भूरि-भूरि प्रशंसा भी कविता के साथ लिखनी होती थी पर वह कुछ इतने क्रूर हृदय होते थे कि सप्ताह बीतते न बीतते ‘सधन्यवाद’ वापस की एक छपी किट कविता के साथ चेंपकर मेरी काव्यकामिनी को मेरी ओर ही धकेल मारते थे। यह लुका-छिपी कुछ इतनी दीर्घसूत्री थी कि मैं अपने कवि होने पर संदेह करने लगा।
कुछ हो कविता में और कुछ हो न हो—एक बात तो होती है कि जब इसकी धुन लग जाती है तो आसानी से छुड़ाये नहीं छूटती। दूसरे-दूसरे सभी कामों से आप कभी-न-कभी भाग खड़े हो सकते हैं पर एक बार कवि कहलाने के बाद आप इसका यश किसी तरह नहीं छोड़ना चाहते।
सहसा इसी समय मेरा भाग्योदय होने का एक आभास मिला। मेरे बड़े भ्राता जो गाँव में रहते थे और अमीनी करते थे, एक दिन कस्बे के घर में आकर बोले, ‘‘ले भाई तेरे कबीर जी (कवि जी) होने की बात तो हमने ऊपर तक पहुँचा दी।’’
मेरे ज्येष्ठ भ्राता मात्र मिडिल पास थे और उन्हें कवि और कबीर में कोई अन्तर मालूम न था। उनके लिए तुलसीकृत रामायण के अलावा और कहीं कविता नहीं थी और तुलसीकृत रामायण को वह भले ही लाल कपड़े में बड़ी श्रद्धा से बाँध-बूँधकर सँभालकर रखते हों पर तुलसी के कवि होने की गरिमा से वह रत्ती-भर प्रभावित नहीं थे। उन ऐसे भक्तप्रवर अनुज से अपने कवि होने की स्वीकृति पाना ही कुछ कम नहीं था—यह जो अपने नाम के ऊपर तक पहुँचने की बात सुनी तो मेरा सिर घूम गया। कई मिनट तो मैं सकते की हालत में रहा कि वह क्या कह रहे हैं पर अन्ततः मैंने सही बात जानने की गरज से उनका चेहरा देखा—पूछा कुछ नहीं। दरअसल उस जमाने में अपने से उम्र में बड़े गुरुजन से कुछ पूछने की परम्परा नहीं थी, इसे बड़ों से ‘जुबान लड़ाना’ समझा जाता था। जो कुछ और जितना कुछ वह बतला-समझा देते थे—काफी समझा जाता था।
मुझे अपनी ओर ताकते देखकर वह गर्व से हँसे और कहने लगे, ‘‘धरपा गाँव का चौधरी एदल सिंह रेडियो स्टेशन पर एक बड़ा अफसर है—डायरेक्टर समझो। मैंने उससे तेरा जिकर किया था। कधी-कधा गाँव में आत्ता रहवे है। कहरा था कि उसे कधी दिल्ली बेज्जो अपनी लिखी कबीता लैके।’’ फिर वह निष्कर्ष देते हुए बोले, ‘‘वो तेरी कविता, रेडियो पै गवा देगा जरूर। इब वैसे बी तू तू कुछ कर तो रहा नी—अपनी कविता ठाके (उठाकर) चला जा किसी दिन—मन्ने तो तेरी भतेरी तारीफ कर रक्खी। न्यूँ बी दिल्ली कुछ घणी दूर तो हैनी।’ किरावा बी कुछ ढेर नी लगता। सुबेरे की गड्डी पकड़ लियो जकशन पै जाके। परोगराम करके रात की टरेन से वापस चल पड़ियो।’’
यह जो रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर साहब से सीधे ही जा मिलने की जुगत निकली तो कई दिनों तक मैं पूरी तरह से बौखलाया घूमता रहा। मैं उन दिनों खद्दर का कुर्ता-पायजामा और जाड़ों में कश्मीरी पट्टू की सदरी जिसे सब जवाहरकट कहते थे—पहना करता था। खूब लम्बा और गोरा-चिट्टा युवक था पर दिल्ली के रेडियो पर बड़े अफसर से मिलने के लिए तो जरा ढंग की पोशाक चाहिए थी। और लिबास भी कुछ ऐसा जो वहाँ की दुनिया में उजबक घोषित न करे।
अब से चालीस-पैंतालीस बरस पहले एक खास कपड़े का सूट पहनने का रिवाज था, उसे गैबरडीन कहते थे। मेरे सौभाग्य से मेरे भाई ओवरसियर थे। पी.डब्लू.डी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट एक सोने का अण्डा देने वाली तगड़ी मुर्गी समझा जाता था और वह उसी में—आज की भाषा में—जूनियर इंजीनियर थे। मेरे भाई-भाभी उस दौरान एक बार हम लोगों से मिलने आये हुए थे। मुझे हल्के से कुर्ते पायजामें में देखकर मेरी भाभी को बड़ी दया आई और उन्होंने तुरन्त अपने बटुए से सौ रुपये का नोट निकाल कर मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, ‘‘भैया जी आप एक सूट बनवा लो गैबरडीन का।’ वह एकदम निरक्षर होते हुए भी आदमी को सूट पहनने पर ही आदमी मानती थीं। मेरा स्वदेशी प्रेम रुपये पाते ही न जाने कहाँ हवा हो गया। मैं उड़ता हुआ कंछीलाल बजाज की दुकान पर गया।। सूट के लिए गैबरडीन कटवाई और कंछीलाल के ठीक सामने वाले शेर खाँ दर्जी, जिसे आम तौर पर मास्टर कहा जाता था, को जा पकड़ाई।
मास्टर शेर खाँ ने एक हफ्ते के बाद ट्राई के लिए आने को कहा और मेरा नाप लेते हुए बोला, कपड़ा कुछ बेसी है—एक टोपी भी निकल आयेगी।’
मास्टर शेर खाँ की बात पर मैं मन ही मन हँसा—यहाँ सूट-टाई पर कौन मरदूद टोपी लगायेगा ? मगर मुझे बाद में यह देखकर तो अनेक बार हैरानी हुई कि हमारे कस्बे में ही नहीं, इस महान देश के बड़े-बड़े नगरों तक में न जाने कितने धर्म-प्राण सूट के नीचे जनेऊ और नेकटाई के बावजूद सिर पर चोटी-टोपी बड़ी शान से धारण करते हैं। यही नहीं किसी मंदिर, शिवालय या दो ईंटे खड़ी करके भूमिया के थान के सामने बाकायदा हाथ जोड़कर श्रद्धाभिभूत हो सिर नवाते हैं।
पहले तो मैंने सोचा, अपने दिल्ली निवासी मित्र कवि शैलेश को पत्र लिखकर रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर चौधरी एदल सिंह के बारे में पता करूँ और हो सके तो उसी के साथ जाकर उस नामी-गिरामी हस्ती के शुभ दर्शन करूँ। शैलेश निश्चय ही उनसे थोड़ा-बहुत परिचित तो होगा ही। फिर उसकी रेडियो स्टेशन तक सहज पहुँच भी थी। उसके साथ जाने पर कहीं भटकने की ज्यादा गुंजाइश भी नहीं थी क्योंकि उसे दिल्ली में रहते दो-ढाई साल हो चुके थे।
परन्तु काफी सोच-विचार करने के बाद मुझे लगा कि शैलेश के साथ चौधरी एदल सिंह जी से मिलने जाना ठीक नहीं होगा। हो सकता है, वह इस बात को पसन्द ही न करें कि उन्होंने मिलने के लिए बुलाया तो मुझे और मैं एक और को साथ टाँग कर ले गया। इसके अलावा मैं गुपचुप ढंग से रेडियो की इस तोप से मुलाकात करके शैलेश पर कहीं यह रोब भी डालना चाहता था कि बच्चू रेडियो से कविताई गाने वाले तुम अकेले तुर्रम खां नहीं हो—मुझे भी रेडियो वाले तुमसे कहीं बेहतर ढंग से घास डालते हैं। मैं चाहता था कि रेडियो से धूमधाम मचाने वाला मेरा एक कार्यक्रम प्रसारित हो जाए तो मैं अपने सहपाठी और प्रतिद्वन्द्वी को ऊँट बनाकर पहाड़ के नीचे से निकाल दूँ।
मैं निश्चित दिन और तारीख पर मास्टर शेर खां की दूकान पर गया और काफी तनते उचकते हुए टेलर मास्टर को सूट की ‘टिराई’ दे आया। रात-दिन सपनों में डूबते-उतराते वक्त गुजर रहा था। हालाँकि मैंने अभी तक रेडियो स्टेशन की इमारत तो क्या उसकी कहीं एक तस्वीर तक भी नहीं देखी थी, मगर मैं अपने मानसिक नेत्रों से उसे सुने-सुनाये भवन के गलियारों और स्टूडियो के चक्कर काटता फिरता रहता था और लौट कर चौधरी एदल सिंह रेडियो स्टेशन डायरेक्टर के शानदार कक्ष में उनके सामने कुर्सी पर जा बैठता था और घोर आत्मीयता से वार्तालाप करता रहता था। मेरा यह हवाई बतियाना जब शिखर पर था तभी एक दिन शैलेश दिल्ली से आ निकला। उसने कस्बे की मानसिकता पर लानत भेजते हुए दिल्ली में अपनी उपलब्धियों की फेहरिस्त मेरे सामने फैला दी। वह वहाँ कितने बड़े-बड़े राजनेताओं और संसद सदस्यों तथा साहित्यकारों से आये दिन मिलता रहता है तथा उसे वहाँ साहित्य का मंच अनायास उपलब्ध होता रहता है, इसका उसने ‘आपन भरनी आपन करनी—विविध मुख बरनी’ की तर्ज पर घंटों बखान किया। उसकी बातों को लनतरानियों का बेसिर का पिटारा मानकर—उसकी बातों पर मैं मन-ही-मन बहुत ऊँचाई पर बैठा हँसता रहा। मैंने उसे रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर से मिलने की इच्छा और योजना की हवा भी नहीं लगने दी। हाँ, चालाकी से यह अवश्य पूछ लिया कि यह भवन दिल्ली में कहाँ स्थित है और इसमें लोग किस तरह दाखिल होते हैं।
शैलेश, अपनी भविष्य निधि के तौर पर फैली अनेक योजनाओं का विराट स्वरूप मुझे दिखाकर दो-चार दिन में ही दिल्ली वापस लौट गया। इधर मैंने भी भाभी से मिले सौ रुपयों का शेषांश—पच्चीस रुपया टेलर मास्टर शेर खां की नजर करके उनके कारखाने से अपना गैबरडीनी सूट उठा लिया। मैं लाख भूलना चाहूँ मगर मास्टर शेर खाँ टोपी-क्षेपक नहीं भूला। उसने सूट लिफाफे में डालने के बाद टोपी मेरे हाथ में देते हुए कहा, ‘‘जनाबेमन शायर साहब, यह टोपी आप की शख्शियत में चार चाँद लगा देगी। माशाल्ला जरा लगाकर तो दिखाइये।’’
टोपी के प्रति घोर वितृष्णा का भाव मन में धीरे-धीरे भी मैंने सामने के आदम-कद आइने में खुद को नापते-तौलते हुए भी सूट से कहीं पहले उस सितम जरीफ़ टोपी को सिर पर चढ़ाकर दाएँ-बाएँ खिसकाया और स्वयं पर सैकड़ों लानतें भेजते हुए उस टोपी को सिर से उतारकर दीवार के सहारे खड़ी सिलाई मशीन पर टिका दिया और वहाँ से यों लपका जैसे कोई जेबकतरा भीड़ में गुम होने के लिए सिर पर पाँव रखकर भाग खड़ा होता है।
सूट मिल जाने के बाद भी मैं तुरन्त दिल्ली नहीं जा सका क्योंकि जिन्दगी में पहली बार मेरा सूट सिला था। उसे पहनने का अभ्यास जरूरी था। मैंने कभी टाई और गर्दन का मेल-मिलाप भी नहीं देखा जाना था—उस स्थिति को भी जानना समझना था। इसके अलावा फ्लैक्स के जूतों की जो एक बड़ी दूकान शहर में थी, उस पर जाकर अपने खुरपे जैसे लम्बे बेडौल पैरों के लिए बूट जुटाने की मुहिम भी सर करनी थी और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि मैं अपने किसी परिचित अथवा मित्र को भी इस डर से अपनी सहायतार्थ नहीं घेर सकता था कि कहीं वह मेरे इस नये शौक का मखौल उड़ाते हुए इसे ‘टाक आफ दा टाउन’ की रंगत न दे दे।
रम्मू फ्लैक्स वाले की दूकान बन्द होने से पहले मैं गली के कोने पर जाकर खड़ा हो गया और जब मैंने देखा, रम्मू के अलावा उसके शोरूम में सिर्फ जूतों पर चँवर डुलाने वाला छोकरा ही बाकी रह गया है तो मैं गली से निकल कर सड़क पर जा निकला और रम्मू के जूतों की अलमारियों के बीच जाकर खड़ा हो गया। अनाज की पूरमपूर दो बोरियों को एक के ऊपर रख दिया जाय तो रम्मू के आकार-प्रकार और आगे बढ़े पेट का कुछ अन्दाज हो सकता है। रम्मू ने अपनी आँखें मिचमिचाते हुए मेरी मंशा की थाह ली और लड़के से बोला, ‘‘छंगा ! बाबूजी को जूता दिखा।’’ पर उसके कण्ठ की घरघराहट से शब्द यों सुनाई पड़े, ‘‘छंगा ! बाजूजी कू जूता सुँघा।’’
किसी तरह ग्यारह रुपये में मुझे पता नहीं किस कम्पनी (फ्लैक्स का जूता) उस जमाने में भी चौदह-पन्द्रह से कम नहीं मिलता था) का बूट रम्मू ने भेड़ दिया। भले ही उसकी दूकान पर फ्लैक्स का जहाजी बोर्ड लगा था मगर माल उसके यहाँ हर छोटी-बड़ी कम्पनी का मौजूद था।
यह एक अलग कहानी है कि उन बूटों ने हफ्तों तक परम शत्रु का व्यवहार ही नहीं किया जब भी मौका पाया मेरे टखनों तक को स्नेहभाव से कुछ इस ढब पर सहलाया कि आज तक टखनों की खाल काफी ऊपर तक खिंच जाने पर भी उन संस्पर्शों से चिह्नित है। एड़ियों की कटाई-मंजाई से उद्भूत छालों की गाथा तो ‘छिल छिलकर छाले फोड़े’ तक भी जा पहुँची थी। बाद में मेरी दीन दशा पर एक प्रत्यक्षदर्शी का सुझाव था कि ऐसे बीहड़ पादत्राणों की मार से बचने के लिए मोटी-तगड़ी जुराबें पहनने का शऊर पैदा करना भी जरूरी है।
कोट की ऊपरी जेब में गुलाबी रूमाल अटकाने से लेकर गले में टाई लटकाने तक के लिए भी बाकायदा एक ‘मास्टर आफ साइंस’ की शिष्यता ग्रहण की जब मैं टाई में किसी तरह भी कायदे की ‘नाट’ नहीं लगा सका तो उन्होंने हारकर सर्पीली धजा वाली टाई को अपने गले में डालकर उसमें गाँठ लगाई और गले से टाई निकालकर मेरे हाथ में देते हुए आजिजी से बोले, ‘‘अब इसे इसी हालत में सँभाल कर रखो। जब पहनने की जरूरत पड़े तो गले में डालकर इसकी निचली पर्त खींच देना—बिल्कुल फाँसी के फन्दे की तरह।’’
सूट-बूट-टाई-रूमाल और जाड़े का मौसम आ जाने की वजह से कोट के बटन होल में गुलाब की कली अटकाने का कई दिनों तक अभ्यास करने के बाद मैंने दिल्ली जाने की सोची। जाने से पहले एक महत्त्वपूर्ण कार्य उन कविताओं और गीतों को ढंग से सँजोना-सँवारना भी था जो ‘आल इंडिया रेडियो’ के स्टेशन डायरेक्टर साहब को सौंपे जाने थे। मैंने बाजार से हल्के नीले कागजों का एक बड़ा पैड खरीदा और कई दिनों तक सुलेख में उन पर बड़ी सधी उँगलियों से अक्षर-अक्षर कविताएँ उभारीं। मैं अपनी कविता की बेड़ियों में चौधरी एदल सिंह को पूरी तरह जकड़ लेना चाहता था।
उस जमाने के हिसाब से जो भी सुन्दरतम हैन्डबैग बाजार में मिल सकता था, उसमें मैंने कविताओं का पैड जमाया और एक छोटी-सी अटैची में एक-दो कपड़े, रूमाल, कंघा आईना और ‘अफगान स्नो’ की शीशी रख ली और एक सुबह घर से दिल्ली विजय के अभियान पर निकल पड़ा।
रिक्शा स्टैण्ड तक मैं कई छोटे-छोटे शार्टकट पार करके पहुँचा और मैंने अपनी आँखें बराबर नीचे झुकाए रखीं। एक तो मैंने इस तरह सरेआम सूट-बूट टाई वगैरह पहले कभी नहीं पहनी थी, दूसरे मैं अपनी शुभयात्रा के आरम्भ में ही किसी की टोका-टाकी का सामना करना नहीं चाहता था।
मैं अपने लिबास को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क था, पर मुसीबत यह थी, कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी मेरे कस्बे से चार मील दूर जंक्शन से मिलती थी। न तो मैं उस लिबास में चार मील धूल-धक्कड़ में पैदल चल सकता था, न ताँगे में बाकी आठ सवारियों के बीच ठुँस सकता था। सड़क की हालत का तो बस कहना ही क्या। हर दस-बारह गज के फासले पर बेमाप गढ़े-गढ़हिया नजर आते थे। शेरशाह सूरी के जमाने में द्द्धी की सड़क थी। कहा जाता है कि जब सन उन्नीस सौ छियालीस में पंडित नेहरू कस्बे में आये थे तो उन्हें दूसरे कई उपहारों के साथ सिख समाज ने सरोपा, एक तलवार भी भेंट की थी। जब पंडित जी का काफिला पंडितजी को इलाहाबाद की गाड़ी पर सवार कराने के लिए जंक्शन की ओर रवाना हुआ तो पंडित जी कार के बार-बार रुकने की वजह जानने के लिए कार से बाहर निकल आए थे और उन्होंने गाँव के कच्चे रास्तों से भी गई-बीती सड़क का जायजा लेते हुए हाथ में पकड़ी हुई तलवार को हवा में लहराते हुए क्रोधावेश में घोषणा की थी, ‘‘अगर किसी दिन मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो मैं इस कस्बे के चेयर मैन को फाँसी लगवा दूँगा।’’
जिस समय का मैं जिक्र कर रहा हूँ तब तक पंडित जी को इस देश का प्रधानमंत्री बने कई साल गुजर चुके थे। एक आम चुनाव भी देश में वर्षों पहले सम्पन्न हो चुका था मगर न तो हमारे कस्बे की म्यूनिसिपैलिटी के चेयर मैन को फाँसी पर चढ़ाया गया था न उस सड़क की हालत में कोई तब्दीली हुई थी। अब मैं जेब में गुलाबी रुमाल दबाये सोच रहा था कि जंक्शन तक बिना धूल का पाउडर पोते कैसे पहुँचूँ। बस एक ही रास्ता था कि भाड़े पर पूरा रिक्शा लूँ और कस्बे से निकलने के बाद सड़क से हटकर पतली-सी पगडण्डी पर हौले-हौले रिक्शा चलवाते हुए जंक्शन तक पहुँचूँ। इसमें बस खतरा यही था कि जिस गाड़ी को पकड़ने की नीयत से मैं घर से निकला था, वह मुझे न मिल पाती। ‘अब जो भी हो—देखा जाएगा’ के भाव से मैंने एक रिक्शाचालक से अकेली सवारी ले चलने की पेशकश की और उस पर सवार होकर चल पड़ा।
जैसा सोचा था वही हुआ। नौ बजे की गाड़ी तो उसी समय छूट गई जब मैं रेलवे स्टेशन से लगभग डेढ़ मील दूर था। अब इलाहबाद की तरफ से ग्यारह बजे के करीब एक डाक गाड़ी आती थी उसी के मिलने की उम्मीद थी। रेलवे स्टेशन पर पहुँच कर मैंने बहुत सावधानी से अपने सूट पर पड़ी धूल की महीन पर्त को हल्के हाथों से झाड़ा और रिक्शा का भाड़ा चुकाकर दिल्ली का टिकट खरीदने खिड़की के सामने पहुँच गया।
साधारण दर्जे का टिकट खरीदने के लिए तब तक छोटे कस्बों के स्टेशनों पर ‘क्यू’ सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। मार ठट्ट के ठट्ठ देहाती और कस्बाई भीड़ टिकट खिड़की पर पिली पड़ रही थी। मैंने भीड़ में घुस कर टिकट खरीदने का जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा। उससे तो मेरे कोट-पतलून का भुरकुस ही निकल जाता। लिहाजा मैंने अपने रिक्शाचालक को एक अठन्नी का लोभ देकर दिल्ली का तीसरे दर्जे का टिकट खरीदवाया। यह बाद की बात है जब रेलवाई ने तीसरे दर्जे के एक डंडे को हटाकर उसे झूठ-मूठ में ही सेकिंड क्लास कर दिया था।
पुरानी दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी से उतर कर मैं प्लेटफार्म पार करके बाहर सड़क पर आया तो बेपनाह भीड़ देखकर बौखला-सा गया। मेरा दिल्ली का भौगोलिक ज्ञान लगभग शून्य था। बहुत साल पहले दिल्ली में जब मेरे भाई सी.पी.डब्लू.डी. में कुछ सालों तक जूनियर इंजीनियर रहे थे तो मैं उनके पास आया था। अब यह भी भूल चुका था कि मैं तब किसके साथ आया था। स्टेशन से कुछ फर्लांग आगे चाँदनी चौक था और वहाँ सड़कों पर तब ट्रामें चलती थीं। मगर सुना था कि इस बीच उनका चलना बन्द हो चुका था और दिल्ली में दूर-दूर तक दिल्ली परिवहन की बसें चलने लगी थीं।
भीड़ में धक्के खाता मैं चाँदनी चौक से कुछ पहले ही ठहर गया। बहुत-सी बसें इधर-उधर दूर तक लम्बी लाइन में खड़ी थीं और उन पर उन स्थानों के नाम भी दर्ज थे जहाँ उन्हें जाना था। दस-पाँच लोगों से पूछताछ करके मैं पार्लियामेण्ट की दिशा में जाने वाली एक बस पर सवार हो गया और लगभग पौन घंटे में आल इंडिया रेडियो की उस विशेष इमारत के सामने जा पहुँचा जो उस समय तक ‘मीडिया’ की दृष्टि से इस देश की नाड़ी कही जा सकती थी।
बस से उतर कर मैंने इधर-उधर देखा और मन की धुकुड़-पुकुड़ पर काबू पाने का असफल प्रयास करते हुए आकाशवाणी भवन के सामने जाकर खड़ा हो गया।
उस क्षण मैंने पाया कि मुझमें आत्मविश्वास की गहरी कमी है और मैं गैबरडीन का बढ़िया सूट धारण करने के बावजूद निपट बेचारा कस्बाई हूँ जो पार्लियामेण्ट की स्ट्रीट की भव्य इमारतों को दीदे फाड़-फाड़ कर देख रहा है और जिसकी हिम्मत इस सीमा तक जवाब दे गई है जो किसी दफ्तर या भवन के गेट में भी नहीं घुस सकता।
कितनी ही देर तक मैं ‘आल इंडिया रेडियो’ की बिल्डिंग के बाहर खड़ा गेट से बाहर भीतर आने-जाने वालों को देखता रहा। अजीब-अजीब हुलियों और पोशाकों वाले लोग आते-जाते दीख रहे थे। किसी स्थूलाकार आकृति वाले के लम्बे और तैलाक्त बाल पीठ पर पड़े थे और प्रशस्त ललाट पर त्रिपुण्ड शोभायमान था तो उसकी बगल में तम्बूरा थामे कोई महामरियल गुड्डे जैसा व्यक्ति ओंठ चियारता हुआ नजर आ रहा था। कहीं कोई सूखी लकड़ी जैसी रमणी गेट के बाहर निकल रही थी तो बंगाली काट का कुर्ता और चुन्नटदार धोती का कोना कुर्ते की जेब में फँसाये बंगाली मोशाय लपकते नजर आ रहे थे। मैंने थोड़ी देर में ही समझ लिया कि अखिल भारतीय आकाशवाणी पर अखिल भारतीय प्रतिभाओं का जमावड़ा स्वाभाविक है। किसी भी आने-जाने वाले को अपने से अलग किसी का अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता था। स्वयं या अपने साथ के लोगों के वजूद के अलावा दूसरों से लगभग सभी पूरी तरह बेखबर थे।
गेट के बाजू में पान की दूकान थी जिस पर खासी भीड़ जमा थी। चूँकि तब तक मेरा पान-बीड़ी-सिगरेट से कुछ लेना-देना नहीं था, इसलिए हिम्मत करके पनवाड़ी से कुछ पूछना भी संभव नहीं था। अन्त में हिम्मत करके एक खाकी वर्दी वाले दरबान या गेटकीपर से मैंने चौधरी एदल सिंह से मिलने की बात कही। वह शख्स भी देहात का रहने वाला क्योंकि उसने अपनी बीड़ी जलाना छोड़कर गौर से मुझे देखा और मेरे सूट के भीतर बदहवास देह-प्राण की मुश्किल का अन्दाज लगाकर भले मानुष का रूख अख्तियार कर लिया। ‘‘लगता है चौधरी के मनई हओ—सूधे जायकै स्टूडियो के दुआर पै पहोंचौ। चौधरी हुंई मिल जाई चहै।’’
मेरी मुश्किल इतनी आसानी से हल हो जायगी, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं समझता था चौधरी एदल सिंह जैसे बड़े और महत्त्वपूर्ण अधिकारी से मिलने में पता नहीं कितनी बाधाएँ उपस्थित होंगी।
मैं आश्वस्त होकर आगे बढ़ते हुए एक लम्बे गलियारे में घुस गया और गलियारे के बीच में खड़े एक खाकी वर्दीधारी अधेड़ से पूछने लगा, ‘‘मुझे चौधरी एदल सिंह जी स्टेशन डायरेक्टकर से मिलना है—क्या बता सकते हैं कि वह कहाँ मिलेंगे ?
भारी-भरकम देह वाले उस रोबीले गेटकीपर ने मुझे पैरों से सिर तक बड़े ध्यान से देखा और फिर उसके चेहरे पर विचित्र-सी मुस्कराहट दीख पड़ी। उसकी मुस्कान में परिहास की कमी नहीं थी। वह गम्भीर होने का प्रयास करते हुए बोला, ‘‘तो डायरेक्टर साहब चौधरी जी से मिलने आये हो।’’
मेरे ‘हाँ’ कहने पर उसने गलियारे से गुजरते अपने जैसे लिबास वाले एक नौजवान को आवाज दी, ‘‘नोखे लाल, इन साब कू डिरेक्टर चौधरी जी के पास तो छोड़ अइयो—देख वहीं स्टूडियो के गेट पै स्टूल पै बैठे होंगे स्यात।’’
गेटकीपर के इन शब्दों का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया कि चौधरी जी स्टूडियो के गेट पै स्टूल पै बैठे होंगे स्यात। पर मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान न देकर नोखे लाल के पीछे चलने की ही कोशिश की।
मैं यह देखकर ताज्जुब में पड़ गया कि गोल गुम्बद के नीचे गोलाकार भाग को पार करते ही स्टूडियो के प्रवेश द्वार पर जो मझले कद का अधेड़ व्यक्ति खड़ा था—नोखे लाल मेरी ओर संकेत करके उससे कुछ कह रहा था।
मैं वहाँ पहुँचा तो वह ताँबई रंग और कद्दावर काठी वाला आदमी जरा आगे बढ़ आया और बोला, ‘‘अमीन साब के लोहरे (छोटे) भैया हो ? उनने मोय बतायो हतौ कि हमाओ भैया कबीर है गयो—वाय कबीता की लत लग गई हतै।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book